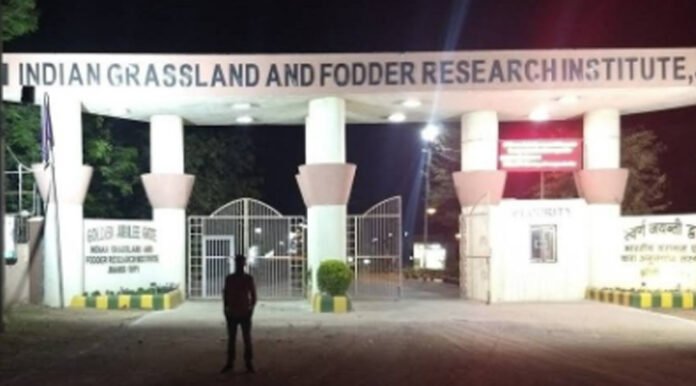भारत तथा कुछ अन्य देशों के हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी आदि सैकड़ों वर्षों से गौहत्या का विरोध करते आये हैं। भारतीय धर्मों में प्राचीन काल से ही गाय सहित अन्य पशुओं की हत्या का व्यापक रूप से निषेध किया जाता रहा है। विशेषरूप से अंग्रेजी शासनकाल में कर्इ ऐसे आंदोलन हुए जो गाय की हत्या रोकने या रुकवाने के उद्देश्य से किये गये थे। 1860 के दशक में पंजाब में सिखों द्वारा किया गया गौरक्षा आंदोलन सुविदित है। 1880 के दशक में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का समर्थन पाकर गौरक्षा आंदोलन और अधिक विस्तृत हुआ। भारतीय मूल के सभी धर्म गौरक्षा का समर्थन करते हैं। गौरक्षा का समर्थन केवल भारत में ही नहीं, श्रीलंका और म्यांमार में भी इसे भारी समर्थन प्राप्त है।
श्रीलंका पहला देश है जिसने पूरे द्वीप पर पशुओं को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने से रोकने वाला कानून पारित किया है। स्वाधीन भारत में विनोबाजी ने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग रखी थी। उसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कानून बनाने का आग्रह किया था। वे अपनी पदयात्रा में यह सवाल उठाते रहे। कुछ राज्यों ने गौवधबंदी के कानून बनाये।
सन 1955 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मलचंद्र चटर्जी (लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पिता) ने गौवध पर रोक के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की कि ‘मैं गौवधबंदी के विरुद्ध हूं। सदन इस विधेयक को रद्द कर दे। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर न तो विचार करें और न कोर्इ कार्यवाही।’ धीरे-धीरे समय निकलता जा रहा था। लोगों को लगा कि अपनी सरकार अंग्रेजों की राह पर है। वह आश्वासन देती रही और गौवंश का नाश होता गया।
इसके बाद 1965-66 में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, स्वामी करपात्री और देश के तमाम संतों ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया। गौरक्षा का अभियान शुरू हुआ। देशभर के संत एकजुट होने लगे, लाखों लोग और संत सड़कों पर आने लगे। इस आंदोलन को देखकर राजनीतिज्ञ लोगों के मन में भय व्याप्त होने लगा। इसकी गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 21 सिंतबर 1966 को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा ‘‘गौवधबंदी के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बारे में आप जानती ही हैं। संसद के पिछले सत्र में भी यह मुद्दा सामने आया था और जहां तक मेरा सवाल है मैं यह समझ नहीं पाता कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश में, जहां गलत हो या सही, गौवध के विरुद्ध ऐसा तीव्र जन-संवेग है गौवध पर कानूनन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता?’’ इंदिरा गांधी ने जय प्रकाश नारायण की यह सलाह नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान ने 7 नंबवर 1966 को दिल्ली में विराट आंदोलन किया। दिल्ली के इतिहास का वह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। जिसमें संसद का घेराव करते कर्इ संत गौरक्षक पुलिस की गोलियों से मारे गये।
12 अप्रैल 1978 को डॉ. रामजी सिंह ने एक निजी विधेयक रखा, जिसमें संविधान की धारा 48 के निर्देश पर अमल के लिए कानून बनाने की मांग थी। संविधान की धारा 48 में यह व्यवस्था है कि राज्य पशुधन विशेषकर गौवध तथा अन्य दुधारू और भार वाहक पशुओं की तस्करी रुकवाने के लिए उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगी। यह राज्यों पर छोड़ा है कि वे लोगों की भावनाओं और रीति-रिवाजों के अनुरूप गौरक्षा के लिए कानून बनाएंगे।
21 अप्रैल 1979 को विनोबा भावे ने अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसार्इ ने कानून बनाने का आश्वासन दिया और विनोबा ने उपवास तोड़ा। 10 मर्इ 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया। इंदिरा जी के दोबारा शासन में आने के बाद 1981 में पवनार में गौसेवा सम्मेलन हुआ। उसके निर्णयानुसार 30 जनवरी 1982 की सुबह विनोबा ने उपवास रखकर गौरक्षा के लिए सौम्य सत्याग्रह की शुरुआत की। वह सत्याग्रह 18 साल तक चलता रहा। लेकिन सरकार के कानों पर जूँ नहीं रेंगी। अन्ततः आज तक गौवध पर केंद्र सरकार किसी भी तरह का कानून नहीं ला पायी है।
बाक्स सन 1966 के अक्टूबर-नवंबर में अखिल भारतीय स्तर पर गौरक्षा आंदोलन चला। भारत साधु समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। 7 नवंबर 1966 को संसद पर हुये ऐतिहासिक प्रदर्शन में देशभर के लाखों लोगों ने भाग लिया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी थी जिसमें अनेक गौ-भक्तों का बलिदान हुआ था। इस गौरक्षा आंदोलन में स्वामी ब्रह्मानंद का विशेष योगदान रहा, इन्होंने प्रयागराज से दिल्ली तक सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल यात्रा की तथा गुलजारी लाल नंदा के आवास को घेरकर अनशन किया। संसद भवन में घुसने के प्रयास पर भयानक लाठी चार्ज का सामना किया। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने ठाना कि गौरक्षा के लिए कानून बनाने को संसद में निर्वाचित होकर आना पडेगा, 1967 में हामीरपुर लोकसभा यूपी से भारतीय संसद में संत सांसद के रूप में निर्वाचित होकर पहुंचे तथा सदन में गौरक्षा के लिए बेबाक राय रखी।