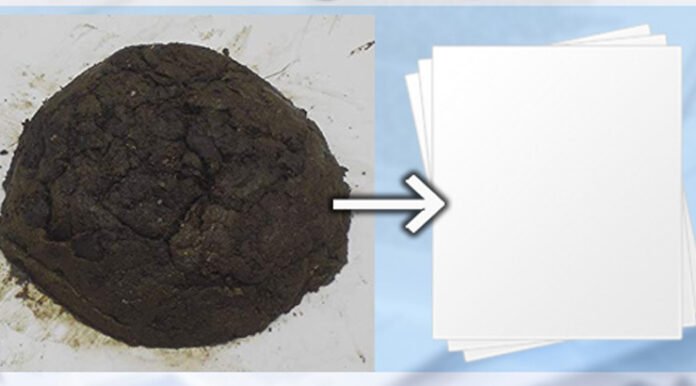देश के तीन राज्यों – तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सबसे अधिक बूचड़खाने हैं. पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया के आंकलन पर गौर करें तो देश में अवैध बूचड़खानों की संख्या अभी भी 30,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। जबकि सूचना का अधिकार (आरटीआर्इ) के जरिये पता चला है कि देश में मात्र 1,707 बूचड़खाने ही पंजीकृत हैं
सबसे अधिक पंजीकृत बूचड़खाने वाले सूबों की फेहरिस्त में क्रमशः तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन स्थानों पर हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ समेत आठ राज्यों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआर्इ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को भारतीय खाद्य संरक्षा एंव मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआर्इ) ने ये आंकड़े फूड लायसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिये उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान किए हैं। आरटीआर्इ के तहत मुहैया कराये गये इन आंकड़ों की रोशनी में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बड़ी तादाद में अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं।
आरटीआर्इ अर्जी पर भेजे जवाब में एफएसएसएआर्इ के एक अफसर ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में एक भी बूचड़खाना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत नहीं है। आरटीआर्इ से मिली जानकारी यह चौंकाने वाला खुलासा भी करती है कि आठों राज्यों में ऐसा एक भी बूचड़खाना नहीं है जिसने केंद्रीय या राज्यस्तरीय लायसेंस ले रखा हो। एफएसएसएआर्इ ने आरटीआर्इ के तहत बताया कि तमिलनाडु में 425, मध्यप्रदेश में 262, और महाराष्ट्र में 249 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं। यानी देश के कुल 55 फीसदी बूचड़खाने इन्हीं तीन सूबों में चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अवैध पशुवधशालाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवार्इ चर्चा में है जबकि प्रदेश में महज 58 बूचड़खाने ही पंजीकृत हैं। आंध्रप्रदेश में 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9, असम में 51, बिहार में 5, छत्तीसगढ में 111, दिल्ली में 14, गोवा में 4, गुजरात में 4, हरियाणा में 18, हिमाचल प्रदेश में 82, जम्मू कश्मीर में 23, झारखंड में 11, कर्नाटक में 30, केरल में 50, लक्षदीप में 65, मणिपुर में 4, और मेघालय में एक बूचड़खाने को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत किया गया है।
ओडिसा में 5, पुडुचेरी में 2, पंजाब में 112, राजस्थान में 84, और उत्तराखंडृ में 22 और पश्चिम बंगाल में 5 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं। एफएसएसएआर्इ ने आरटीआर्इ के तहत यह भी बताया कि देशभर में 162 बूचड़खानों को प्रदेश स्तरीय लायसेंस मिले हैं, जबकि 117 पशुवधशालाओं को केंद्रीय लायसेंस हासिल है। इस बीच पशुहितैषी संगठन पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की विज्ञप्ति में मोटे आंकलन के हवाले से कहा गया है कि देश में अवैध या गैरलाइसेंसी बूचड़खानों की संख्या 30,000 से ज्यादा है।
हालांकि, कर्इ लायसेंसशुदा बूचड़खानों में भी पशुओं को बेहद क्रूरतापूर्वक जान से मारा जाता है। पेटा इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे ऐसी पशुवधशालाओं को बंद कराएं जिनके पास उपयुक्त प्राधिकारणों के लायसेंस नहीं है और जो कानून द्वारा निषिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।